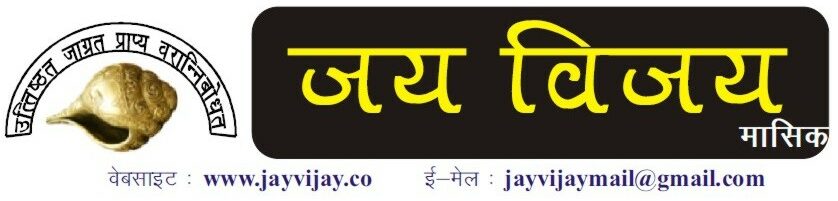एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण:- श्रीमद्भगवद्गीता धार्मिक ग्रंथ ही नही अपितु विज्ञान भी
श्रीमद्भगवद्गीता भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला आध्यात्मिक ग्रन्थ है। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है । गीता में ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग व राजयोग के अतिरिक्त समत्वं योग, सन्यास योग, सांख्य योग, श्रद्धात्रय योग व मोक्ष का अद्भुत संगम है। भागवत गीता में धार्मिक और आध्यात्मिक उपदेशों के साथ-साथ कई वैज्ञानिक और दार्शनिक सिद्धांत भी निहित हैं। यहां कुछ श्लोकों के माध्यम से हम भागवत गीता के इन वैज्ञानिक पहलुओं की व्याख्या करेंगे:-
श्लोक:: अध्याय 2, श्लोक 13,
“देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति।।”
अर्थ: जैसे इस देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। धीर पुरुष इस पर विचलित नहीं होते।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण: यह श्लोक शरीर और आत्मा के परिवर्तनशील और स्थिर तत्वों की चर्चा करता है। जैविक दृष्टिकोण से, शरीर कोशिकाओं के निरंतर पुनर्नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है, जो कि एक प्रकार का शारीरिक परिवर्तन है।
श्लोक :: अध्याय 2, श्लोक 22,
“वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही।।”
अर्थ: जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण: यह श्लोक शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को दर्शाता है, जो पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुरूप है। पुनर्जन्म का सिद्धांत कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे ऊर्जा के संरक्षण से मेल खाता है, जिसमें ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल रूपांतरित किया जा सकता है।
श्लोक:: अध्याय 2, श्लोक 47,
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।।”
अर्थ: तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्मफल की चिंता किए बिना कर्म करो।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण: यह श्लोक निष्काम कर्म की शिक्षा देता है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी महत्वपूर्ण है। शोधकर्ता निष्पक्षता से काम करते हैं और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कार्य को पूरा करते हैं।
श्लोक:: अध्याय 3, श्लोक 9,
“यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर।।”
अर्थ: यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म बंधन का कारण होते हैं। इसलिए, मुक्त भाव से कर्म करो।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण: यह श्लोक सामूहिक प्रयास और समाज के हित में कार्य करने का महत्व बताता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में भी, व्यक्तिगत लाभ से परे सामूहिक और सामाजिक हित को प्राथमिकता दी जाती है।
श्लोक:: अध्याय 3, श्लोक 16,
“एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः।
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति।।”
अर्थ: जो इस चक्र का पालन नहीं करता, वह पापयुक्त, इंद्रियों का दास और व्यर्थ जीवन जीता है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण: यह श्लोक प्राकृतिक नियमों और चक्रों के पालन का महत्व बताता है। जैसे वैज्ञानिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है, वैसे ही नैतिक और सामाजिक नियमों का पालन करना भी आवश्यक है।
श्लोक:: अध्याय 5, श्लोक 18,
“विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः।।”
अर्थ: जो विद्या और विनय से सम्पन्न हैं, वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल में समान दृष्टि रखते हैं।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण: यह श्लोक सभी प्राणियों में समानता और समता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यह जैव विविधता और प्रजातियों की समानता के सिद्धांत के अनुरूप है।
श्लोक:: अध्याय 6, श्लोक 5,
“उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः।।”
अर्थ: आत्मा द्वारा आत्मा का उद्धार करो, आत्मा को पतित न होने दो। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण: यह श्लोक आत्म-संयम और आत्म-निरीक्षण के महत्व पर बल देता है, जो मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
श्लोक:: अध्याय 9, श्लोक 22,
“अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।।”
अर्थ: जो लोग अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूँ।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण: यह श्लोक समर्पण और ध्यान की महत्ता पर बल देता है, जो मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ध्यान और समर्पण मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन में सहायक होते हैं।
श्लोक:: अध्याय 10, श्लोक 20,
“अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः।
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च।।”
अर्थ: हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ, जो सभी जीवों के हृदय में स्थित है। मैं ही सभी प्राणियों का प्रारंभ, मध्य और अंत हूँ।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण: यह श्लोक सार्वभौमिक चेतना और अस्तित्व की अवधारणा को दर्शाता है, जो आधुनिक भौतिकी में ब्रह्मांडीय चेतना और अंतर-संबंधों के सिद्धांतों के साथ मेल खाता है।
श्लोक:: अध्याय 13, श्लोक 16,
“अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्।
भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च।।”
अर्थ: वह अविभाज्य है, फिर भी समस्त प्राणियों में विभाजित के समान स्थित है। वह जानने योग्य, प्राणियों का धारण करने वाला, निगलने वाला और उत्पन्न करने वाला है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण: यह श्लोक क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों के समान है, जिसमें ऊर्जा और पदार्थ की अविभाज्यता और उनका परस्पर संबंध दर्शाया जाता है।
निष्कर्षतः इन श्लोकों के माध्यम से, भागवत गीता न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक उपदेश प्रदान करती है, बल्कि जीवन के विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं की भी व्याख्या करती है।।
— डॉ. पंकज भारती