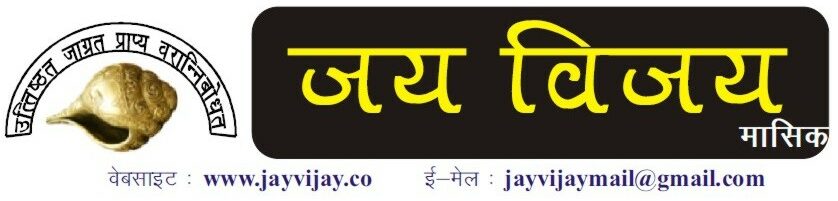उन्नत तकनीक और भविष्य की खेती
कृत्रिम मेधा यानी एआइ का बढ़ता उपयोग और इसका प्रभाव आज चर्चित मुद्दा है प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिनों पहले पेरिस में आयोजित ‘एआइ सिक्योरिटी समिट’ के दौरान सार्वजनिक, निजी और शैक्षणिक हितधारकों से एक विश्वसनीय एआइ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए मिल कर काम करने का आह्वान किया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि एआइ हमारे काम करने के तरीके को बदल देगा। विश्व आर्थिक मंच का अनुमान अनुमान कि एआइ 2027 तक विश्व स्तर पर आठ करोड़ तीस लाख नौकरियों को खत्म कर देगा। एआइएमफ की रपट की मानें तो एआइ के कारण दुनियाभर में लगभग 40 फीसद नौकरियां प्रभावित होंगी। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, तो हमारा देश, जो कृषि परंपराओं से जुड़ा हुआ है, आज एक तकनीकी क्रांति के कगार पर खड़ा है भारत अपनी विशाल आबादी और विविध अर्थव्यवस्था के कारण अद्वितीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। अगर ठीक से प्रबंधित किया जाए, तो एआइ में उत्पादकता, दक्षता और रोजगार बढ़ाते हुए इन चुनौतियों से लड़ने की अपार क्षमता है।
ऐसे समय में जब सबसे ज्यादा चर्चा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों पर स्वचालन (आटोमेशन) और एआइ के प्रभाव पर केंद्रित है, तब कृषि क्षेत्र रहा तकनीकी परिवर्तन न केवल उत्पादकता, बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने की अपार क्षमता रखता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य देशों की तुलना में कम होने के बावजूद, पूरी दुनिया को खाद्यान्न संकट से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। नीति निर्धारकों को यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है भारत में रोजगार का भविष्य केवल प्रौद्योगिकी के विघटनकारी प्रभावों को कम करने पर निर्भर नहीं है, बल्कि रणनीतिक से विकास रास्ते बनाने के लिए कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में इसकी शक्ति का उपयोग करने पर निर्भर करने पर निर्भर है।
पीढ़ियों से, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करती है। हालांकि, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कई चुनौतियों से ग्रस्त है। जैसे, अप्रत्याशित मानसून खंडित जीत और कीमतों में उतार-चढ़ाव इन मुद्दों ने कृषि संकट और बेहतर अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्रों 1 में पलायन में योगदान दिया है। इस परिदृश्य में एआइ की शुरुआत इन चुनौतियों समाधान करने, उत्पादकता बढ़ाने और इस प्रक्रिया में कृषि कार्य के लिए एक नई पीढ़ी बनाने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करती है।
यह स्वाभाविक है कि स्वचालन से बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो N जाएंगी, लेकिन, भारतीय कृषि के संदर्भ में, एआइ से मानव क्षमता बढ़ने की अधिक संभावना है, न कि उन्हें पूरी तरह से बदलने की संभावनाओं पर अगर विचार करें, तो एआइ- संचालित सेंसर मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी, मौसम की अधिक सटीकता से भविष्यवाणी और सिंचाई के समय को अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे बढ़ी हुई पैदावार और संसाधनों की बर्बादी में कमी हो सकती है एआइ से लैस ड्रोन विशाल खेतों का सर्वेक्षण कर सकते हैं और कीटों या बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। यहां तक कि लक्षित उपचार भी दे सकते हैं, जिससे व्यापक कीटनाशक अनुप्रयोग की आवश्यकता कम हो जाती है। ये प्रौद्योगिकियां मानव भागीदारी की आवश्यकता को खत्म नहीं करतीं, बल्कि काम की प्रकृति को बदल देती हैं।
कृषि में एआइ के एकीकरण से विभिन्न क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग पैदा होगी। हमें कृषि इंजीनियरों की आवश्यकता है, जो एआइ-संचालित मशीनरी और सिंचाई प्रणालियों को डिजाइन करें और बनाए रख सकें। हमें डेटा वैज्ञानिकों की आवश्यकता है, जो इन प्रणालियों द्वारा उत्पन्न विशाल डेटा का विशेषण कर सकें। हमें कृषि कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता है, जो प्रौद्योगिकी और किसानों के बीच की खाई को पाट सकें, जटिल डेटा को व्यावहारिक सलाह में बदल सकें। हमें साफ्टवेयर डेवलपर की आवश्यकता है, जो विशिष्ट कृषि आवश्यकताओं के लिए एआइ ऐप बना सकें। हमें ड्रोन पायलटों की आवश्यकता है जो इन महत्त्वपूर्ण उपकरणों का संचालन और रखरखाव कर सकें। संभावनाएं विशाल और विविध हैं।
इसके अलावा, कृषि में में एआइ का अनुप्रयोग सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे रोजगार के अवसरों का और विस्तार हो सकता है। किसानों को सीधे बाजारों से जोड़ने के लिए एआइ-संचालित मंचों श्रृंखला प्रबंधन और ई-कामर्स में नई भूमिकाएं के विकास से रसद, आपूर्ति पैदा हो सकती हैं। हालांकि, इस | क्षमता को साकार करने के लिए सभी हितधारकों को ठोस प्रयास करने की का प्रयास आवश्यकता है सक्षम वातावरण बनाने में सरकार की की भी बड़ी | भूमिका है। । इसमें कृषि एआइ में अनुसंधान और विकास में किसानों को इन तकनीकों को अपनाने के लिए सबसिडी और प्रोत्साहन प्रदान करना तथा कार्यबल को आवश्यक कौशल से लैस प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना शामिल है। ‘एग्रीटेक’ कंपनियों के लिए निजी क्षेत्र को भी इसमें भूमिका निभानी होगी। ‘एग्री- छोटे किसानों की जरूरतों के अनुरूप किफायती और सुलभ एआइ समाधान विकसित करने की आवश्यकता है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए किसानों और विश्वविद्यालयों के साथ मिल के साथ मिल कर काम करने की कृषि जरूरत है कि ये प्रौद्योगिकियां उपयोगकर्ता के अनुकूल और प्रभावी हों कई किसानों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता तक पहुंच की कमी है। ग्रामीण ब्राडबैंड बुनियादी ढांचे और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में निवेश के के माध्यम से इस अंतर को पाटना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कृषि में एआइ के लाभ सभी किसानों तक पहुंचें। इसमें न केवल प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करना शामिल है, बल्कि किसानों को इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षित शिक्षित करना भी शामिल है।
तकनीकी पहलुओं से परे, इस परिवर्तन के सामाजिक और आर्थिक सामात निहितार्थी को संबोधित करना भी महत्त्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि छोटे सीमांत किसान इस तकनीकी क्रांति में पीछे न रहें। सामूहिक खेती का समर्थन करने, ऋण और बीमा तक पहुंच प्रदान करने और बाजार संबंधों को बढ़ावा देने | देने वाली नीतियां छोटे किसानों को एआइ- संचालित कृषि से लाभान्वित होने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा, उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल बनाना आवश्यक है, जो एआई के कारण हाशिए पर जा सकते हैं, भले ही हम नई नौकरियां पैदा करें। भारतीय कृषि में कृत्रिम मेधा का भविष्य किसानों को रोबोट से बदलने बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें उन उपकरणों और ज्ञान के साथ सशक्त बनाने बारे में है, जिनकी उन्हें तेजी से बदलती दुनिया में पनपने के लिए आवश्यकता है। एआइ को अपना कर और अपने कार्यबल के कौशल में निवेश कर, हम भारतीय कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और न्यायसंगत क्षेत्र में बदल सकते हैं। कृषि क्षेत्र में एक नई पीढ़ी बना सकते हैं। सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यह परिवर्तन सिर्फ फसलें उगाने के बारे में नहीं है, यह भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य की खेती करने के बारे में है।
— विजय गर्ग