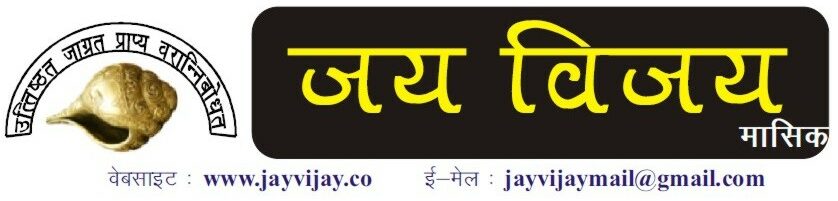रूढ़ि या प्रथा
बढ़ते आधुनिकता के दौर में रूढ़िप्रथा को लोग एक तरह के अभिशाप (कुप्रथा) के रूप में मानते हैं, या इन शब्दों की विविधताओं को उजागर करने से बचते हुए नजर आते हैं । बहुत सारे लोगों में इसके प्रति घृणा, अस्वीकृति के भाव प्रकट होते हैं । इसके प्रति लोगों में यह धारणा व्याप्त हो चुकी है कि, यह प्रथा गाँव – देहात और पिछड़े हुए लोगों की संस्कृति है और हम पिछड़े हुए लोग नहीं है या उनकी विधान का समर्थन नहीं करते । उन्हें पता होना चाहिए कि रूढ़िवादी प्रथा कभी समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे समाप्त करने का पर्याप्त विकल्प मौजूद नहीं है जो आदि अनंत कालों से चली आ रही है।
रूढ़ि जन्य प्रथा का आशय_
यह एक ऐसी विचारधारा या दृष्टिकोण है जो पारंपरिक मूल्यों प्रथाओं और संस्थाओं को महत्व देता है और बदलाव के प्रति संदेहास्पद है। रूढ़ियों का प्रयोग उन सामाजिक नियमों व्यवहारों या विश्वासों को दर्शाने के लिए किया जाता है । जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं और अक्सर बदले नहीं जाते । प्राचीन काल से पुरखों से चली आ रही सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रथा को “रूढ़िप्रथा” कहते हैं । जो आज भी बनी हुई है जिसका विरोध नहीं कर सकते और अगर इसे हटा दिया जाए तो सामाजिक समीकरण गड़बड़ा जाएगा और बाजार बाद हावी हो जाएंगे। रूढ़िवादिता वहां सिद्धांत है जो अधिकांश आबादी के पास है, जो सामूहिक विशेषताओं को साझा करते हुए सांस्कृतिक मूल्यों रीति – रिवाजों और परंपराओं को महत्व देकर संरक्षित कर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
धार्मिक स्वरूप में रूढ़िवाद _ अगर शहरों को छोड़ दिया जाए तो यह प्रथा, परंपरा सदियों से ग्राम समाज में व्याप्त है जो विभिन्न लोक पर्व में झलकता हैं । ग्रामों में बारह जाति के बाना – बानीधारी लोग (पारधी, कुम्हार, तेली मरार गोंड, कोष्टा, लोहार, यादव, गाड़ा, घसिया आदि ) मिलाकर ग्रामीण परंपरा, संस्कृति को संपादित करते हैं । छत्तीसगढ़ के लोक पर्व “अक्ती” (बीज परीक्षण ) से लेकर वर्षांत त्योहार “होली” में भी रूढ़िप्रथा समाहित है । गांव में कोई भी देवी- देवता साकार रूप में साक्षात नजर नहीं आते बिना हाथ – पैर, आँख – कान वाले (पराशक्ति ) को मानते हैं । प्रायः इन देवी – देवताओं का देवालय नहीं पाए जाते हैं । ग्राम के देवी- देवता को जमीन पर विराजमान होने का अधिकार है । इनके अलावा किसी भी देवी – देवताओं को गांव में बसने का अधिकार नहीं है । वह अतिथि के तौर पर आते जाते रहते हैं, अब आजकल कहीं-कहीं देखा जाने लगा है की माता देवाला के त्रिशूल, बाना के स्थान पर मूर्ति पधारे जा रहे हैं, तो कहीं पर साड़हा देव के स्थान पर दूसरी मूर्ति को स्थापित करने लगे हैं । यह अज्ञानता का प्रतीक है, इससे ग्रामीण संस्कृति में विकृतियाँ आने लगी है । ज्योति- जंवरा के स्थान पर आप बिजली के बल्ब नहीं जला सकते, ठाकुर देव को अनाजों के स्थान पर मिठाईयाँ अर्पण नहीं कर सकते घर पर मुखिया के रहते हुए दूसरे के सर पर पगड़ी नहीं बाँध सकते । गांव की देवी – देवता का विधि विधान सर्वथा मौखिक में है, लिखित में नहीं । रूढ़ि प्रथा जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कार में भी विद्यमान है ।
रूढ़ि चिन्ह_ किसी विशिष्ट संरचना या विशिष्ट संकेत आदि को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं और उसी संदर्भ में रूढ़ (स्थिर) हो जाते हैं जैसे_ सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड, यातायात के संकेतक चिन्ह, नक्शे, नदी, तालाबों, पेड़, पहाड़, त्रिशूल बाना, ध्वजा, बैरग, खंभा देव ठाना बाना, पुरखों के मठ (गुडी) खटला पूजा, पीढ़ी पूजा, अर्पण, तर्पण, समर्पण के भाव प्राकृतिक शक्तियाँ आदि हो सकते हैं।
रूढ़ि ताकतें _ घर्षण, वायु प्रतिरोध, चिपचिपाहट, तनाव, खिंचाव, धरती, आकाश, पानी वायु, अग्नि के प्रभाव को समझना मौसम आधारित कार्य करना, स्प्रिंग, गुरुत्वाकर्षण बल आदि।
रूढ़िगत उदाहरण_ 1) कुछ क्षेत्रों में विवाह के लिए विशेष रीति रिवाज को रूढ़ियाँ कहा जा सकता है । (2) लिंग के आधार पर व्यवहार को नियंत्रित करने वाली रूढ़ियाँ हो सकती हैं, कुछ लिंग आधारित नेग, दस्तूर है। (3) कुछ सांस्कृतिक समूह में विशिष्ट प्रकार के भोजन समारोह को मनाने की रूढ़ियाँ हो सकती है। (4) एक ऐसी स्थिति जहां चीज स्थिर रहती हैं और बहुत या कम या कोई बदलाव नहीं होता।
मानवगत रूढ़ियाँ _
(1) जैसे दलितों के बारे में उच्च जाति के मन में एक विशेष प्रतिमा बन गई है कि जिसके आधार पर वे दलितों को गंदे, अनपढ़, नि:सहाय कमजोरी आदि समझते हैं। (2) सभी मुस्लिम आतंकवादी होते हैं वे दंगा फैलाते रहते हैं। ( 3) एक धारणा आदिवासी नक्सली होते हैं भले ही मानवता पूर्ण तरीके से व्यवहार करते हो वह वास्तव में एक शांतिप्रिय व्यक्ति हो । ( 4) किसी जाति, धर्म नस्ल के लोगों को दूसरों से कमतर समझने नस्ली भेदभाव का कारण बन सकता है। सामाजिक असमानता छोटा- बड़ा समझना । (5) लोगों के मन में धारणा है भगवान साधु के भेष बनाकर भीख मांगने आते हैं, भगवान की कृपा से मनुष्य सुखी और दुखी होते हैं। (6) नींबू मिर्च, झाड़ू, टीका लगाने से जादू टोना गायब होते हैं । (7) हुम – धूप, अगरबत्ती, मोमबत्ती, नमस्कार, चमत्कार से जीवन में बदलाव आते हैं। जाति धर्म के आधार पर पदों का निर्धारण करना एक रूढ़िवादी धारणा है।
निष्कर्ष_
सामाजिक रूढ़िवादी व्यवस्था उदारवाद का समर्थन नहीं करता इस व्यवस्था में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही भाव हैं । रूढ़िवादी प्रथा को जड़ से समाप्त नहीं कर सकते ग्रामीण समाज की नीति नियम, विधि – विधान, बिगड़ जाएंगे पुरखों की प्राचीन संस्कृतियाँ विलुप्त हो जायेंगी, लोग जात से बेजात हो जाएंगे जन्म लेने के पश्चात जीव- जंतु, पशु- पक्षियों की तरह बंधन मुक्त आजाद हो जाएंगे । किन्तु व्यक्ति के सार्वजनिक विकास के लिए रूढ़ियों का त्याग होना चाहिए जाति – धर्म वर्ण, रंग – रूप के आधार पर भेदभाव समाप्त हो, शासन प्रशासन के कार्यों में समानता हो सभी व्यक्तियों को मुख्य पदों पर आसीन होने का समान अवसर मिले सभी के धर्म संस्कृतियों, रीति – रिवाजों का रक्षा और उचित सम्मान होना चाहिए।
— मदन मंडावी