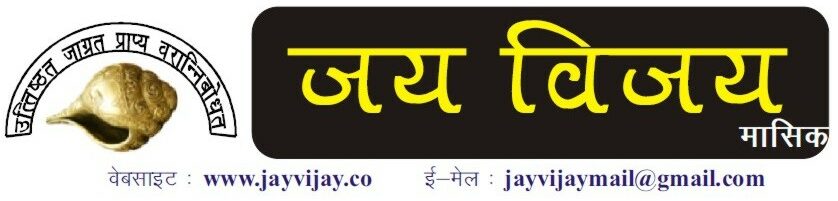शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता
स्वामी विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ, हावड़ा में हुई। विवेकानन्द वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक देशभक्त संन्यासी थे। वे आध्यात्मिक विकास तक सीमित नहीं थे। वे अपने देशवासियों की दरिद्रता से पीड़ित होते थे और उनके भौतिक विकास की आकंाक्षा ही नहीं, निरंतर प्रयास करते रहे। स्वामी जी भूखे व्यक्ति के लिए भजन की नहीं रोटी की चिंता करना आवश्यक समझते थे। उन्होंने नर सेवा को नारायण सेवा मानने का आह्वान किया। पाश्चात्य देशों की यात्राओं के समय उन्होंने भारत की आध्यात्मिक संपन्नता का पक्ष रखते हुए उन्हंे आध्यात्मिक ज्ञान देने व भौतिक ज्ञान लेने की चर्चाएं की थीं। स्वामी जी ने पाश्चात्य जगत को आध्यात्मिक शिक्षा देने व उनसे भौतिक शिक्षा लेने का आह्वान किया। स्वामी जी भौतिक रूप से लगभग 123 वर्षो से हमारे बीच नहीं हैं, किन्तु उनके महत्वपूर्ण विचार, हमें निरंतर मार्गदर्शन देते रहे हैं और देते रहेंगे। उन्होंने शिक्षा को व्यक्ति के विकास का आधार माना था। उन्होंने सभी को शिक्षित करने पर जोर दिया। स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि हमें महिलाओं के कल्याण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें शिक्षित कर दें, अपने कल्याण की चिंता वे स्वयं कर लेंगीं।
कई्र बार हमें लगता है कि स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबन्धी विचार उस समय व परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सही रहे होंगे, वर्तमान में परिस्थितियाँ काफी भिन्न हैं और स्वामी जी के शिक्षा संबन्धी विचार प्रासंगिक नहीं रहे। उस समय शैक्षणिक दृष्टि से हम पिछड़े हुए थे। साक्षरता दर नाम मात्र ही थी। वर्तमान में हम शत-प्रतिशत साक्षरता की ओर बढ़ रहे हैं। तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सूचना व प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान की दृष्टि से हम विश्व के अग्रणी देशों में गिने जाने लगे हैं।
निःसन्देह! परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है किंतु स्वामी जी के शिक्षा संबन्धी विचार परिस्थितियों पर आश्रित नहीं थे। उनके विचार सार्वकालिक थे, हैं और रहेंगे। हमें आवश्यकता यह समझने की है कि उन विचारों को वर्तमान संदर्भ में समझें। कुछ विचार अमर होते हैं। वे सदैव ही उपयोगी और प्रासंगिक होते हैं। स्वामी जी के विचार भी कुछ इसी प्रकार के थे। आओ! उनके शिक्षा संबन्धी विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता पर विचार करें।
स्वामी जी की शिष्या भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के विचार में शिक्षा को इस प्रकार से स्पष्ट किया है, ‘‘भारतीय शिक्षा की किसी समस्या को हल करने के लिए, सबसे पहले सामान्य शिक्षा कार्य का अनुभव होना आवश्यक है; और इसके लिए शिक्षार्थी की आँखों से संसार की ओर – चाहे वह क्षण भर के लिए ही क्यों न हो- देखते रहना सब से बड़ा और नितान्त वांक्षनीय गुण है। शिक्षार्थी की आकांक्षाओं के विपरीत शिक्षा देना, भलाई की अपेक्षा दुष्परिणामों का निश्चित रूप से आह्वान करना है।’’ इन विचारों की प्रासंगिकता पर विचार करें तो ये सार्वकालिक हैं। ऐसा कोई भी समय हो ही नहीं सकता कि ये विचार उपयोगी न रहें। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम शिक्षा अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप ही पाना चाहते हैं। हमारी आकांक्षाओं का गठन हमारी पारिवारिक व सामाजिक आकांक्षाओं से होता है। जब हम आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करते हैं, तब हम व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक उन्नति करने में सक्षम होते हैं। समाज में शान्ति व आनंद का वातावरण सृजित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम होते हैं।
स्वामी जी का विचार था कि हमारे यहाँ के बालकों को निषेधात्मक या अभावात्मक शिक्षा दी जाती है। उसमें कुछ अच्छी बातें तो हैं, पर उसमें एक ऐसा भयंकर दोष है, जिसके कारण वे सारी अच्छी बातें दब जाती हैं। पहले तो, वह मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही नहीं है। वह पूर्णतया निषेधात्मक शिक्षा मात्र है। निषेधात्मक शिक्षा या कोई भी प्रशिक्षण जो निषेध पर आधारित हो, मृत्यु से भी बदतर है। स्वामी जी के इन विचारों के सन्दर्भ में हम वर्तमान समय में प्रचलित शिक्षा को देखते हैं तो विद्यालयों में यह सुनाई देता है, ‘यह मत करो। यह अनुशासन के खिलाफ है। अनुशासनहीनता करोगे तो विद्यालय से निकाल दिया जाएगा।’ विद्यार्थियों को यह कहा जाता है कि वे ‘यह न करें’ किन्तु यह नहीं सिखाया जाता कि वे ‘यह करें।’ उन्हें क्या और क्यों करना चाहिए यह शिक्षा व्यवस्था में कहीं दिखाई नहीं देता। संस्कारों की दुहाई दी जाती है किन्तु स्वयं शिक्षक और अभिभावक अपने आचरण से विद्यार्थियों को संस्कार नहीं दे पाते। केवल निषेध बताया जाता है। सकारात्मक रूप से यह नहीं सिखाया जाता कि उन्हंे क्या और क्यों करना है? अभी भी निषेधात्मक शिक्षा ही दिखाई देती है। अतः स्वामी विवेकानंद का सकारात्मक शिक्षा के आह्वान को हम आज तक अपनी शिक्षा व्यवस्था में शामिल नहीं कर पाए हैं। वे आज भी न केवल प्रासंगिक हैं, वरन उन पर काम करने की आवश्यकता है।
स्वामी जी ने शिक्षा के संबन्ध में कहा था, ‘शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है, जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूँस दिया गया है और जो आत्मसात् हुए बिना वहाँ आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है, जो जीवन-निर्माण, मनुष्य-निर्माण और चरित्र-निर्माण में सहायक हों। यदि तुम पाँच ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हो, तो तुम एक पूरे ग्रन्थालय को कण्ठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो।’’ स्वामी विवेकानंद के इन विचारों का महत्व जरा भी कम नहीं हुआ है। वास्तविकता भी यही है कि हम अपने विद्यालयों में शिक्षा दे ही नहीं रहे हैं। उन्हें केवल कुछ जानकारियाँ रटाकर डिग्रियाँ दे रहे हैं। हम अपने विद्यार्थियों को शिक्षा न देकर साक्षर बनाकर केवल कुछ जानकारियाँ रटा रहे हैं, जो जीवन में उनके किसी काम की नहीं होतीं।
शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षण के दौरान भावी शिक्षकों को यह रटाया अवश्य जाता है कि व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ही शिक्षा है किन्तु उनके व्यवहार में ही कोई परिवर्तन नहीं होता। शिक्षक स्वयं ही शिक्षित नहीं होता। ऐसी स्थिति में विद्यालयों में जाकर वह शिक्षा कैसे दे सकता है? जिसके पास जो है ही नहीं, उसको वह और किसी को कैसे दे सकता है? स्वामी जी के विचारों के आधार पर अपनी शिक्षा प्रणाली को विकसित करके ही हम जीवन-निर्माण, मनुष्य-निर्माण और चरित्र-निर्माण करने में सहायक हो सकते हैं। इस दिशा में बहुत काम करने की आवश्यकता है। स्वतंत्र भारत में तीन-तीन शिक्षा नीतियाँ बनाने के बावजूद हम अभी तक बहुत अधिक नहीं कर पाए हैं।
स्वामी जी ने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी की थी, ‘‘विदेशी भाषा में दूसरे के विचारों का रटकर, अपने मस्तिष्क में उन्हें ठूँसकर और विश्वविद्यालयों की कुछ पदवियाँ प्राप्त करके, तुम अपने को शिक्षित समझते हो! क्या यही शिक्षा है? तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? या तो मुंशीगिरी मिलना, या वकील हो जाना, या अधिक से अधिक डिप्टी मैजिस्ट्रेट बन जाना, जो मुशीगिरी का ही दूसरा रूप है-बस यही न?’’ बस यही न? आज भी प्रासंगिक है। पद नाम भले ही बदल गए हों। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य आज भी नौकरी करना ही दिखाई देता है। कितना भी समय बीत गया हो? कितनी भी शिक्षा नीतियाँ बनाई हों? नौकरी ही केंद्र में बनी हुई है। जीवन-निर्माण, मनुष्य-निर्माण और चरित्र-निर्माण जैसे विषयों का शिक्षा से दूर-दूर तक का नाता नहीं है। यही कारण है कि नैतिक अधमता के स्तर तक अपराधों में वृद्धि हो रही है। हम समाज, देश और मानवता की बात तो करते हैं किंतु व्यवहार में उनसे शायद ही किसी का सरोकार हो।
स्वामी जी कहते हैं, ‘हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, जिससे चरित्र बने, मानसिक वीर्य बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आवश्यकता इस बात की है कि हम विदेशी अधिकार(वर्तमान संदर्भ में अधिकार के स्थान पर प्रभाव लिया जा सकता है) से स्वतंत्र रहकर अपने निजी ज्ञान भण्डार की विभिन्न शाखाओं का और उसके साथ ही अँग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन करें। हमें यांत्रिक और ऐसी सभी शिक्षाओं की आवश्यकता है, जिनसे उद्योग धंधों की वृद्धि और विकास हो, जिससे मनुष्य नौकरी के लिए मारा-मारा फिरने के बदले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त कमाई कर सके और आपत्काल के लिए संचय भी कर सके।’ वर्तमान संदर्भ में देखने पर स्पष्टया समझ सकते हैं कि स्वामी जी ने न तो अंग्रेजी का विरोध किया है और न ही पाश्चात्य विज्ञानों का। हाँ! वे भारतीयता को बनाए रखकर पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान व तकनीकियों का अध्ययन करने की बात करते थे। वर्तमान संदर्भ में भी हमारी शिक्षा नीतियाँ इसी पर जोर दे रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी स्वामी जी की आकांक्षाओं को ही सम्मिलित किया गया है।
स्वामी जी स्पष्ट कहते थे। हम मनुष्य बनाने वाला धर्म चाहते हैं। हम मनुष्य बनाने वाले सिद्धांत चाहते हैं। हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा चाहते हैं। आज स्वामी जी के संसार त्याग के 123 वर्ष बाद भी हम मनुष्य बनाने वाली शिक्षा प्रणाली की स्थापना नहीं कर पाए हैं। वास्तविकता यही है कि हम धर्म, देश, समाज आदि की बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, किंतु हम स्वयं अपने आपको मनुष्य बनाने का प्रयास ही नहीे करते। हम देश के लिए शहादत देने वाले देशभक्त बनाने वाली शिक्षा की अपेक्षा तो करते हैं, किन्तु देश के लिए जीने वाले नागरिक तैयार करने में अक्षम रहेे हैं। हम दूसरों के लिए जीने की बात तो करते हैं किंतु ईमानदारी से अपने आपको समझने व अपने लिए जीने में सक्षम हो पाने वाली शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाते। स्वामीजी अपने पैरों पर खड़े करने वाली शिक्षा देने का आह्वान करते थे किंतु वर्तमान में हम उन्हें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि वे अपने लिए खाना भी नहीं जुटा पाते और खाने के लिए भी सरकारी सहायता पर निर्भर हैं।
हमारी सरकार 80 करोड़ लोगों को पोषण सहायता और भोजन देने की बात गर्व के साथ स्वीकार करती है। राजनीतिक पार्टियाँ लोकतंत्र व गरीबों की सहायता के नाम पर मुफ्त वस्तुएँ व बैंक खाते में सीधे निर्धारित रकम देने की घोषणा, अपने-अपने घोषणा पत्रों और संकल्प पत्रों में करती हैं। महात्मा गांधी भी कहते थे कि किसी व्यक्ति को खाने के लिए चावल उपलब्ध कराने की अपेक्षा उसे चावल उगाने में सक्षम बनाना अधिक उपयोगी है। स्वामी विवेकानंद के विचार में शिक्षा के अन्तर्गत जो जीवन-निर्माण, मनुष्य-निर्माण और चरित्र-निर्माण होना चाहिए, क्या वह हम वास्तव में कर पा रहे हैं? इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी शिक्षा का क्या मतलब है? जो अपनी रोजी-रोटी कमाने में सक्षम नहीं बना पा रही है और सरकार मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी समय-समय पर इस विषय पर चिंता व्यक्त की जाती रही हैं। उनके अनुसार वर्तमान में हम परजीवी नागरिकों का एक बड़ा वर्ग तैयार कर रहे हैं। वास्तव में ऐसी स्थिति में हमें स्वामी विवेकानन्द के शिक्षा संबन्धी विचारों को पुनः वर्तमान संदर्भ में समझने, उन्हें आत्मसात करने और लागू करने की आवश्यकता है। वे आज न केवल प्रासंगिक हैं वरन स्वामी जी के समय से भी अधिक उपयोगी हैं।
टिप्पणी- उपरोक्त आलेख में स्वामी जी के विचारों को, श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर द्वारा ‘स्वामी विवेकानन्द’ नाम से प्रकाशित पुस्तक के सप्तम संस्करण जिसमें स्वामी जी के विचारों पर आधारित आठ आलेखों को स्थान दिया गया है, से लिया गया है।