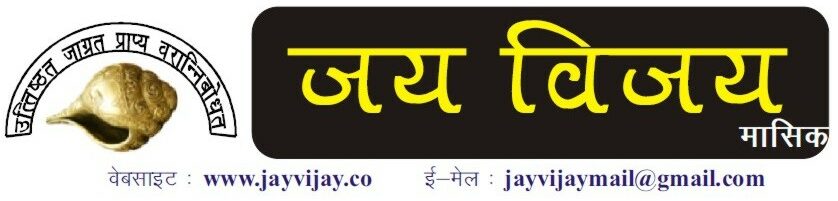कविता और काम का कोई गुरु नहीं होता
काव्य-प्रणयन की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को ‘काव्य हेतु’ या काव्य का कारण कहा जाता है। ये साधन ही कवि को काव्य-प्रणयन में सक्षम बनाते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य या कविता के लिए प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास ये तीनों ही हेतु या कारण बताए गए हैं। ये तीनों एक साथ मौजूद होने पर ही काव्य का निर्माण होता है। कवि की प्रतिभा या शक्ति के अभाव में काव्य का प्रसार या अवतरण सम्भव नहीं है।
चूँकि कविता काव्य का ही भेद है इसलिए ये हेतु कविता प्रणयन के लिए भी आवश्यक हैं, किन्तु कविता अपने आप में एक अवतरण भी है। इसका अवतरण होना ही इसे विशेष बनाता है। विशेष होने से इसके हेतुओं में कुछ और भी है जिनकी चर्चा आवश्यक है। ऐसा स्वत: सभी को आभासित भी होता है। अतः यहाँ इसके हेतुओं पर चर्चा व कविता और काम के प्रणयन पर विचार करना इस आलेख का अभीष्ट है ।
रचना के अवतरण की एक प्रक्रिया होती है। यह एक स्वाभाविक घटना होती है, जिसे अच्छे-अच्छे कवि भी नहीं जान पाते और घटना घट जाती है अर्थात रचना हो जाती है। रचना के अवतरण के उपरान्त कवि को जिस आनन्द की अनुभूति होती है, वह अनिर्वचनीय व वर्णनातीत होती है। अवतरण की यह प्रक्रिया जानबूझ कर न होकर कवि के मानस में अनायास और स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। समाधिस्थ कवि की उपज होने से इसकी उत्पत्ति पर किसी तर्क की कहीं गुंजाइश ही नहीं होती साथ ही अवतरण की इस पूरी प्रक्रिया में गुरु की कहीं भी आवश्यकता महसूस ही नहीं होती।
आइए पहले भाव और विचार में मोटा अन्तर समझते हुए विषय को गति देते हैं। भाव तो सभी के हृदय में जन्म लेते हैं लेकिन आलम्बन के सहारे जब कवि के अन्त:करण में बीज रूप भाव जन्म लेते हैं, तब कवि शनै: शनै: समाधि अवस्था में पहुँच जाता है और वह कल्पना लोक में भ्रमण करता है। जहाँ भावानुकूल होने पर वह परकाया प्रवेश भी कर सकता है। कवि मन की यही अवचेतन अवस्था भी होती है।
कल्पना लोक तो कल्पना लोक है, जहांँ शब्द शक्तियों व काव्य के बाह्य और आन्तरिक तत्त्वों के सहयोग से अकल्पनीय कविता का सृजन पल्लवित होकर अवतीर्ण होता है। यह अवतरण अत्यन्त क्लिष्ट होते हुए भी अति सहज व अनायास होता है। अतः कविता की रचना प्रक्रिया में समाधि और कल्पना को भी मैं कविता के हेतु मानता हूँ। इस तरह प्रतिभा, निपुणता, अभ्यास, समाधि और कल्पना को मिला कर कविता के कुल पाँच हेतु (कारण/साधन) बनते हैं।
ऊपर कह चुका हूंँ कि अवतरित होने से कविता तर्क से परे हो जाती है। यों तो प्रकृति में कमल खिलता है और मनुष्य हँसता है लेकिन तर्क से परे होने के कारण कवि का कमल पुष्प प्रकृति के विपरीत हँस भी सकता है और मनुष्य खिलखिला सकता है। इस पर कोई आपत्ति नहीं लेता क्योंकि जब इसकी व्याख्या की जाती है तब स्पष्ट किया जाता है कि कवि का आशय कमल के खिलने और मनुष्य के हँसने से ही है। वहीं विचार मस्तिष्क में सतत् चलने वाली प्रक्रिया की उपज होते हैं। मस्तिष्क का विषय होने से हर विचार तर्क की कसौटी पर तुला हुआ होता है। मस्तिष्क में हर विचार को तर्क शक्तियों के माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है।
दूसरी बात यह है कि विचार में प्रायः अभिधा शब्द शक्ति प्रधान होती है। यद्यपि यह जरूरी शर्त नहीं है। अन्य शब्द शक्तियाँ भी अपना कार्य करतीं हैं लेकिन विचार में कुछ भी लपेटने से दूसरी शब्द शक्तियों का बोलबाला होने का खतरा रहता है, जिससे विचार का आशय बदल भी सकता है। अतः इसकी तार्किक स्थिरता में परिवर्तन की कोई गुंजाइश कम ही होती है। विचार को तर्कानुशासन की कसौटी पर कसे जाने के कारण कमल पुष्प हँस नहीं पाता, उसे खिलना ही पड़ेगा। मनुष्य खिलखिला नहीं सकता उसे हँसना ही पड़ेगा। तर्क से विचारों की पुष्टि होने के कारण कोई विचार विषाद जन्य भी हो सकता है जहाँ आनन्द की प्राप्ति न हो। इसमें ज्ञान की विशेष आवश्यकता होती है।
अपवाद स्वरूप गद्य में कुछ आलेख कहानी आदि ऐसे आ सकते हैं, जिनमें भावों की प्रधानता हो सकती है, जैसे मुंशी प्रेमचन्द की कहानियाँ, ललित निबन्ध आदि, वहीं कविताएँ भी ऐसी हो सकतीं जिनमें भावों की शून्यता हो और विचारों की प्रधानता हो जैसे आयुर्वेद में लिखे गए श्लोक आदि। इनमें औषधि और रोगों से सम्बन्धित कथ्य रहेगा। इनमें भावों से भरी कल्पना को स्थापित नहीं किया जा सकता अतः कविता के दर्शन ही नहीं होंते। इतना सब कुछ होते हुए भी अनुभव के आधार पर विचार और भाव का अन्तर समझ में आ जाता है।
इसे अन्य उदाहरण से भी समझते हैं जैसे उन्हत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चुहत्तर पचत्तर छियत्तर सतत्तर अठत्तर इसमें लय भी है तुक भी है तान भी है क्रम भी है सार्थकता भी है। लेकिन यह भाव भरी कविता नहीं है वहीं दूसरा उदाहरण देता हूँ। हन्दी में तिरेसठ तेतीस और छत्तीस के अंकों को ऐसे ६३,३३,३६ लिखा जाता है। किसी अज्ञात कवि का एक दोहा है, जिसमें एक सखी दूसरी सखी को बता रही है कि हे सखी! रात को मैं अपने पति से नाराज़ हो गई। अब आगे ६३ , ३३, ३६ के अंकों की बनावट (आकृति) देखकर अर्थ आप स्वयं लगाइए –
“बात बात में रात सखि, गई पिया सों रीस।
त्रेसठ से तेतिस भई,तेतिस से छत्तीस।।”
इस दोहे में वे ही अंक अर्थ के ऐसे विस्फोटक बन गए हैं जैसे ध्वनि काव्य में स्फोट होता है।
निश्चय ही काव्य कर्म बहुत कठिन साधना है किन्तु आश्चर्य ही है कि कवि मन में इस जटिल कविता का सहज ही अवतरण होता है। यह कवि को मिला ईश्वरीय वरदान है। इस वरदान के बल पर एक समर्थ कवि गहरी अथवा उथली बात भी आसानी से कह लेता है। जिस कठिन बात को बड़े-बड़े विद्वान् नहीं कह पाते हैं उसे एक कवि छोटी सी रचना के द्वारा कह जाता है। इतना ही नहीं उसे कालजई बना देता है और एक दीर्घ अन्तराल के बाद कवि स्वयं की रचना पर भी विस्मित होते हुए आश्चर्य व्यक्त कर सोचने लगता है कि यह मैंने कैसे और कब लिख दिया?
शाब्दिक और व्याकरण की दृष्टि से देखें तो संस्कृत के तीन शब्द ऐसे हैं जो काम और कविता के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रणय,प्रणयन और प्रणीत तीनों में पहला और दूसरा शब्द काम के प्रबोधन के लिए व दूसरा और तीसरा शब्द काव्य रचना के लिए प्रयुक्त होता है। प्रणय में प्र उपसर्ग है नी धातु है अच् प्रत्यय है, वहीं प्रणयन में प्र उपसर्ग है नी धातु है ल्युट् प्रत्यय है तो प्रणीत में प्र उपसर्ग है नी धातु है क्त प्रत्यय है। इन शब्दों में कविता और काम दोनों के लिए प्रयुक्त यहाँ एक ही धातु है ‘नी’ । नी धातु के कई अर्थों में एक अर्थ लाना भी है। लाने का अभिप्राय रचना लाने से भी है और परिणय बन्धन से भी। दोनों में ही नव सृजन को लाया जाता है।
अवतरण है तो यह कवि के लिए नैसर्गिक है। नैसर्गिक क्रियाओं के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती। जैसे शरीर से पसीना निकलना एक नैसर्गिक क्रिया है इसमें गुरु की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वत: निकलता है। काम भी नैसर्गिक है, वह भी स्वत: उद्भूत होता है। इसे भी सिखाया नहीं जाता। अल्प बुद्ध पशुओं की वृत्तियों से इसे और भी आसानी से समझा जा सकता है। दोनों ही स्वाभाविक प्रक्रियाएँ हैं इसलिए प्रणय और प्रणयन में गुरु की आवश्यकता नहीं है। अतः स्पष्ट है कि कविता और काम का कोई गुरु नहीं हो सकता।
अब आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कविता का कोई गुरु नहीं होता है तो कवियों में गुरु परम्परा तो बहुत प्राचीन है फिर गुरु किसलिए ? इसका उत्तर यह है कि अवतरण का कोई गुरु नहीं होता लेकिन जिस प्रकार प्रसूता की कोख से बालक के जन्म लेने पर डॉक्टर की निगरानी में नर्सों या घर पर दाई आदि के द्वारा नव प्रसूत बालक के शरीर का शोधन किया जाता है, उसे स्वस्थ और जीवित रखने के लिए उपाय बताए जाते हैं।
ठीक वैसे ही कवि की हृदय पेटी से कविता का अवतरण तो होता है लेकिन अवतरित होने पर उसका भी श्रृंगार किया जाता है, छ्न्द आदि अनुशासन की दृष्टि से अवतरण में भी कई दोष हो सकते हैं जो भावगत अथवा शिल्पगत हो सकते हैं जिनका शोधन किया जाना आवश्यक होता है। जिन्हें कवि अपनी क्षमता से दूर करता तो है किन्तु अज्ञानता बस उन्हें समग्रता से दूर नहीं कर पाता है। ऐसे में आवश्यकता होती है एक सफल मार्गदर्शक अथवा गुरु की, जो हर दोष का हरण कर उसे परिमार्जित और संशोधित करा दे।
बाद में कवि को भी उसे सँवारने के लिए कला सीखनी पड़ती है। स्वयं को कविता का समीक्षक होना पड़ता है। यह कला सतत् अभ्यास और दीर्घ अनुभव से आती है किन्तु उसमें सन्देह भी रहता ही है। इसलिए कवि के लिए काव्य शिल्प में पारंगत गुरुओं की आवश्यकता होती है। कारण छन्द साधना का अत्यन्त जटिल होना भी है। कलागत शिल्प के सौन्दर्य की आभा को निखारने की विद्या मात्र एक गुरु ही दे सकता है क्योंकि कविताओं में उसके बाह्य और आन्तरिक तत्वों व छन्दानुशासन को बचाए रखना रंग और रूप से कविता के आवरण को बचाए रखना होता है।
ईश्वर ने संसार को लयबद्ध किया है। कवि काव्य के द्वारा समाज को लयबद्ध करता है। वह हास्य और उपहास का माद्दा रखता है तो श्रृंगार से लेकर वीभत्स तक के कथ्य में भी सभी को आनन्द देता है। अपनी कल्याणकारी और सन्देश परक रचनाओं से मानवता में नैतिकता का संचरण करता है वहीं उसे सकल सृष्टि के स्वास्थ्य की चिन्ता करनी होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कविता के शिल्प के स्वास्थ्य के लिए गुरु आवश्यक भी है।
— गिरेन्द्रसिंह भदौरिया “प्राण”