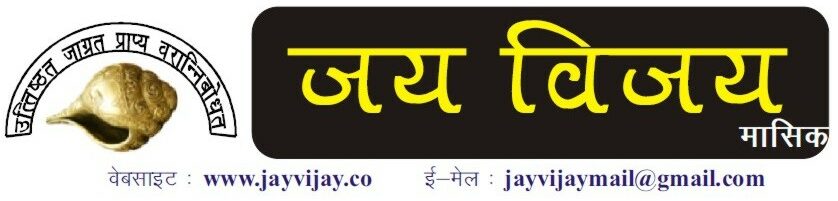जैव विविधता की समृद्धि का आधार है आर्द्र भूमि
प्रकृति जीवों-पादपों की पोषक है, सांसों का स्पंदन है। प्रकृति की रचना में जीवन का सौंदर्य एवं लास्य नर्तन है। ऊंचे उठे नभ छूते गिरि शिखरों पर हिम की रजत चादर हो या पर्वतों से जीवन धारा बन निकली बलखाती चंचल सरिताएं हों। तमाम पशु-पक्षियों एवं मानव को भोजन, आश्रय एवं जीवनोपयोगी संसाधन भेंट करते समृद्ध कानन हों या सतत गर्जना करते उत्ताल लहरों से लोक को नाना प्रकार के रत्नों के उपहार बांटते रत्नाकर महासागर हों। पशु-पक्षियों की क्षुधा मिटाते घास के विस्तीर्ण मैदान हों या फिर नागफनी जैसे कंटीले पौधों के रंग-बिरंगे फूलों से सजा रेगिस्तान। प्रकृति की यह वैविध्यपूर्ण बनावट धरती में जीवन गढ़ती है, रचती है। नदी, झील, डेल्टा, घाटी, जल, जंगल, पर्वत, पठार, उदधि, उपवन, रेत, खेत इन सभी में सौंदर्य बिखरा पड़ा है जो मानव मन को आकर्षित करता है। लेकिन प्रकृति की तमाम अद्भुत रचनाओं में से एक रचना पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, हम उसके महत्व एवं पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी भूमिका से सर्वथा अपरिचित हैं और वह अप्रतिम प्राकृतिक संरचना है आर्द्र भूमि अर्थात धरती का नमी वाला क्षेत्र। वायुमंडल में जलवाष्प की उपलब्धता, आंधी-तूफान और सागरीय चक्रवात, वर्षा एवं वायु विक्षोभ आदि का आधार भूमि की आर्द्रता ही होती है, यह हममें से बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आर्द्र भूमि के महत्व एवं योगदान से परिचित कराने हेतु वैश्विक आयोजन प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस के रूप में किया जाता है। रामसर सम्मेलन में हुई संधि की 54वीं वर्षगांठ हम 2025 में मना रहे हैं।
इसके पहले कि मैं आर्द्र भूमि दिवस मनाने के उद्देश्यों, जीवों-पादपों के जीवन चक्र पर आर्द्रता के पड़ने वाले प्रभावों एवं पारिस्थितिकी तंत्र की बनावट-बसाहट पर बात करूं, मुझे लगता है कि आर्द्र भूमि को समझना समीचीन होगा। आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र अंतर्गत धरती का वह विशेष क्षेत्र होता है जो आंशिक या पूर्णतः वर्ष भर, न्यूनतम आठ महीने, प्रायः जल में डूबा रहता है और जहां जलीय पादपों एवं जल-जीवों की तमाम प्रजातियां विकसित होकर इको सिस्टम को समृद्ध करती हैं। एक प्रकार से भरपूर नमीयुक्त यह दलदली भूभाग जलीय एवं स्थलीय जैव विविधता का मिलन बिंदु या संधि क्षेत्र होता है। दुर्भाग्य से मानवीय दख़ल एवं हस्तक्षेप से सम्पूर्ण विश्व में आर्द्र भूमि पर संकट उभरा है जो न केवल मानव जीवन बल्कि पूरे जीव-पादप विकास एवं जैव जीवन पर खतरा बनकर मंडरा रहा है, क्योंकि आर्द्र भूमि का खत्म होना या क्षेत्र कम होना पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक चक्र को अस्थिर कर देगा और तब तमाम जीव-पादप प्रजातियां विलुप्त हो जायेंगी। इस दृष्टि से विचार करके 2 फरवरी, 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरान के रामसर नगर में आर्द्र भूमि के संरक्षण, युक्तिसंगत उपयोग एवं तत्संबंधी वैश्विक जागरूकता के लिए आयोजित सम्मेलन में एक समझौता हुआ जिसे रामसर संधि कहा जाता है। जिसमें कहा गया कि प्रत्येक देश अपने यहां नेचुरल वेट लैंड अर्थात् प्राकृतिक आर्द्र भूमि को चिह्नित करेगा। ऐसे चिह्नित सभी स्थल रामसर साइट कहे जायेंगे और उनकी एक समग्र वैश्विक सूची बनाई जायेगी। वर्तमान समय में इस सूची में 171 देशों की 2300 से अधिक आर्द्र भूमियों का अंकन किया गया है। संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम में हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमरीकी देश बोलविया शीर्ष पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एवरग्लेड्स वेटलैंड विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट है। इसके साथ ही इन सूचीबद्ध रामसर आर्द्र भूमियों में से ऐसे स्थल जो मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण एवं तकनीकी विकास के कारण बड़े बदलावों का शिकार हुए या हो रहे हैं, उन्हें मोंट्रिक्स रिकार्ड नामक एक पंजिका में अंकित कर संरक्षण के विशेष प्रयास किये जाने हेतु योजना बनाई गयी है और सरकारी एजेंसियों एवं पर्यावरण मुद्दे पर केंद्रित स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा योजनानुसार संरक्षण कार्य किये जा रहे हैं। मोंट्रिक्स रिकार्ड सूची में भारत के दो आर्द्र स्थल शामिल हैं। वर्ष 1990 में केवलादेव घना पक्षी बिहार, भरतपुर (राजस्थान) तथा 1993 में लोमतक झील मणिपुर को संकटग्रस्त रामसर साइट के रूप में पहचाना गया। रामसर सम्मेलन के 26 साल बाद 2 फरवरी, 1997 को पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया।
रामसर संधि के तहत समुद्र स्तर से 6 मीटर ऊंचा ज्वार-भाटा आच्छादित तटीय क्षेत्र एवं गहरे धान क्षेत्र, डेल्टा, झीलें आदि आर्द्र भूमि अंतर्गत शामिल हैं। विश्व की एक अरब आबादी का जीवन यापन आर्द्र भूमि पर ही निर्भर है। वहीं भूमि आधारित कार्बन के 30 प्रतिशत हिस्से का स्रोत भी यही वेट लैंड साइट ही है। आर्द्र भूमियों के महत्व को हम युनेस्को के एक कथन से समझ सकते हैं कि आर्द्र भूमि पर खतरा उत्पन्न होने से विश्व की 40 प्रतिशत वनस्पतियां एवं जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो इन आर्द्र भूमियों पर पाये जाते हैं और प्रजनन करते हैं। विश्व की भू सतह का 6 प्रतिशत हिस्सा आर्द्र भूमि है। भारत के संदर्भ में देखें तो 4.6 प्रतिशत भूमि नमीयुक्त है जिसके अंतर्गत 47 रामसर साइट शामिल हैं जो लगभग ग्यारह लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र को आच्छादित करती हैं। इनमें चिल्का झील उड़ीसा, नंगल एवं रोपड वेटलैंड पंजाब, भिंडावास अभयारण्य हरियाणा, कांवर झील बिहार, अष्टमुड़ी केरल, दीपोर आर्द्र भूमि असम, सांभर झील राजस्थान, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर पक्षी विहार, राजस्थान), स्तार्ता सापुक लद्दाख, भोज आर्द्र भूमि मध्यप्रदेश आदि सहित बिजनौर गंगा बैराज का क्षेत्र हैदरपुर जो वर्ष 2021 में ही इस सूची में शामिल किया गया है। इनमें हिमाचल एवं लद्दाख सहित उत्तरी ठंडे एवं शुष्क क्षेत्र, दक्षिण का तटीय क्षेत्र, मानसूनी वन प्रदेश, बाढ़ वाले मैदानी इलाके, डेल्टा एवं झीलें आदि सम्मिलित हैं। 4230 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है तो हिमाचल का रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा मात्र 0.2 वर्ग किमी क्षेत्र। उल्लेखनीय है कि रामसर संधि भारत में फरवरी 1982 से लागू हुई। आर्द्र भूमियों के उचित संरक्षण एवं रख-रखाव के लिए एक केंद्रीय कानून आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के अंतर्गत सुनियोजित ढांचा विकसित किया गया है। 2 फरवरी, 2021 को आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र स्थापित कर आर्द्र भूमियों की आवश्यकता, अनुसंधान, संरक्षण एवं सम्बंधित ज्ञान-सूचना को परस्पर साझा करने के ठोस प्रयास शुरू किये गये। वर्ष 2025 के आयोजनों की थीम है – हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण।
वास्तव में आर्द्र भूमि जीव-पादप के समुचित विकास का आधार बन जैव विविधता को पुष्टि प्रदान करती है। यहां से कच्चा माल, दवा, वनस्पतियां, आहार आदि की प्राप्ति होती है तो वहीं यह पर्यावरण को साफ-सुथरा रखने में भी सहायक है। यह कचरे के छानने हेतु प्राकृतिक छन्ने का काम करती है। जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के प्रभाव को कम कर पीने का पानी के स्रोत भी हैं। अति संवेदनशील ये स्थल उन जलीय वनस्पतियों एवं मछलियों को पनपने का अनुकूल परिवेश देते हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। इस प्रकार आर्द्र भूमियां एक प्रकार से जीवन को संवारती-सजाती है। हमारा कर्तव्य है कि हम भी इन आर्द्र भूमियों को संभालें-संवारें और आगामी पीढ़ी को समृद्ध जैव विविधता पूर्ण खिली-महकती दुनिया सौंपें।
— प्रमोद दीक्षित मलय