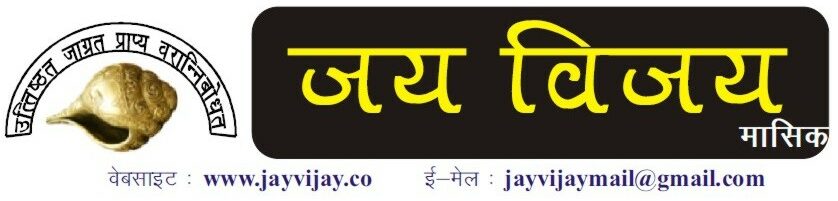भीख मांगने की प्रथा: मदद की गुहार या एक सुनियोजित धंधा?
भारत में भीख मांगना धार्मिक दान से जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्या बन गई है। व्यस्त सड़क पर, हाथ बढ़ाना मदद के लिए पुकार जैसा लग सकता है, लेकिन इसमें अक्सर व्यवस्थित उपेक्षा, संगठित अपराध और शोषण का जाल छिपा होता है। सहानुभूति जीतने के लिए नशीले पदार्थ दिए जाने वाले शिशुओं से लेकर स्कूल से उठाकर सड़कों पर फेंक दिए जाने वाले बच्चों तक, भीख मांगना सिर्फ़ मदद के लिए पुकार से कहीं ज़्यादा है; यह हमारी सामूहिक कमज़ोरियों की आलोचना है। बाल भिखारी अभी भी इस समस्या का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए, यह ज़रूरी है कि इन बच्चों को संरक्षित और शिक्षित किया जाए। कमज़ोर, ख़ास तौर पर बच्चे और विकलांग लोगों का संगठित भीख मांगने वाले गिरोहों द्वारा फ़ायदा उठाया जाता हैं। भिक्षा देने से जुड़ी प्रथाएँ अक्सर भीख माँगने को बढ़ावा देती हैं। अधिक उद्देश्यपूर्ण दान को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक शिक्षा पहल शुरू करना ज़रूरी है।
भारत में सार्वजनिक रूप से भीख मांगने की प्रथा मनरेगा और स्माइल जैसे व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बाद भी आम है। आंकड़ों के अनुसार, 413 लाख से अधिक लोग अभी भी इस प्रथा में लिप्त हैं, जो दीर्घकालिक गरीबी, कम साक्षरता और सरकारी हस्तक्षेप के बावजूद काम के अवसरों की कमी जैसी अंतर्निहित सामाजिक आर्थिक कमजोरियों को रेखांकित करता है। बड़े बच्चों को भीख मांगना सिखाया जाता है, जबकि शिशुओं को बीमार दिखने के लिए नशीला पदार्थ दिया जाता है। कुछ ने कभी कक्षा में क़दम नहीं रखा है और कई ने जल्दी पैसे कमाने के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगाकर स्कूल छोड़ दिया है। हाल के आँकड़े बताते हैं कि भारत में स्कूल छोड़ने वाले बच्चे कितने आम हैं, खासकर किशोरों में। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 18 वर्ष की आयु के 25 प्रतिशत बच्चे बुनियादी पढ़ने के कौशल से जूझते हैं और 32.6 प्रतिशत स्कूल छोड़ देते हैं। विकलांग लोगों का फायदा उठाया जाता है क्योंकि वे भिखारी के तौर पर अधिक पसंद किए जाते हैं। जब मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का इलाज़ नहीं किया जाता है, तो लोग शोषण और निर्भरता के चक्र में फंस जाते हैं।
भारत में 400, 000 से ज़्यादा नियमित भिखारी रहते हैं; उनकी दुर्दशा कई तरह के कारकों से उपजी है, जिसमें संगठित भीख मांगने वाले गिरोह, गरीबी, विकलांगता और प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन शामिल हैं समाज के सबसे कमज़ोर सदस्यों को शिकार बनाकर और लगभग दंड से मुक्त होकर काम करके, इन सिंडिकेट ने ग़रीबी को एक लाभदायक उद्यम में बदल दिया है। 81, 000 से ज़्यादा भीख मांगने वाले लोगों के साथ, पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाला राज्य है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। गरीबी, ग्रामीण-शहरी प्रवास और आसानी से सुलभ सहायता नेटवर्क की कमी इन क्षेत्रों में भिखारियों की बढ़ती संख्या में योगदान देने वाले कुछ सामाजिक-आर्थिक कारक हैं। भारत में, कई कल्याणकारी कार्यक्रमों के अस्तित्व के बावजूद भीख मांगने की प्रथा जड़ जमाए बैठी सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियों के कारण बनी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कल्याणकारी कार्यक्रम अक्सर खराब क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार और प्राप्तकर्ताओं के बीच जागरूकता की कमी के कारण विफल हो जाते हैं। स्माइल जैसी योजनाएँ, जो आश्रय और आजीविका सहायता प्रदान करती हैं, कई भिखारियों को अच्छी तरह से ज्ञात नहीं हैं।
विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी झुग्गियों में, जो लोग घोर ग़रीबी में जी रहे हैं, उनके पास जीवित रहने के लिए भीख माँगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार, मनरेगा जैसे ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ भी, 413, 000 से अधिक लोग भीख माँग रहे थे। भीख माँगने वाले व्यक्तियों में अक्सर औपचारिक शिक्षा और रोजगार योग्य कौशल की कमी होती है, जो औपचारिक रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुँच को सीमित करता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पेश किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण से भिखारियों और अन्य हाशिए के समूहों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुँचा जा सका है। ट्रांसजेंडर लोग और विकलांग लोग कमज़ोर समूहों के दो उदाहरण हैं जिन्हें समाज द्वारा उपेक्षित किया जाता है और मुख्यधारा के आर्थिक अवसरों से बाहर रखा जाता है। कई लोग ट्रैफ़िक सिग्नल पर भीख माँगने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि उन्हें ट्रांसजेंडर कल्याण कार्यक्रमों के बावजूद भी स्वीकार नहीं किया जाता है। कमज़ोर लोगों को आपराधिक नेटवर्क द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो फिर उन्हें भीख माँगने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे इस चक्र को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली में पुलिस ने 2023 में पचास बच्चों को बचाया, जिन्हें तस्करी के गिरोह द्वारा भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया था।
भारत में भीख मांगने की प्रवृत्ति के बने रहने का एक मुख्य कारण यह है कि यहाँ कोई केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं है जो भीख मांगने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास में मदद करने के लिए केंद्रित हस्तक्षेप की अनुमति दे सके। राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए नगरपालिका रिकॉर्ड का उपयोग करने का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सुझाव भिखारियों के बारे में भरोसेमंद जानकारी की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ग़रीबी और भीख मांगने पर निर्भरता तब बनी रहती है जब भीख मांगने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा तक पहुँच से वंचित कर दिया जाता है। आउटरीच पहलों की कमी के कारण, कई बच्चे अभी भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नामांकित नहीं हैं। मादक द्रव्यों के सेवन और अनुपचारित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण लोग भीख मांगते हैं और ग़रीबी में रहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सलाह स्माइल कार्यक्रम के तहत आश्रय गृहों में नशामुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं की कमी को उजागर करती है। बेरोजगारी के कारण ग्रामीण-से-शहरी प्रवास के कारण शहरी भीड़भाड़ के कारण, प्रवासियों को भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भीख मांगने के खिलाफ कानून संगठित अपराध से निपटने और पुनर्वास प्रदान करने के लिए या तो कठोर हैं या अपर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, जबरन भीख मांगने वाले नेटवर्क को जन्म देने वाले अंतर्निहित मुद्दों को सम्बोधित करने के बजाय भिखारियों को अपराधी बनाता है।
भारत में भीख मांगने से निपटने के लिए नीतियाँ, लक्षित कल्याण हस्तक्षेपों को सुविधाजनक बनाने और उनके पुनर्वास को ट्रैक करने के लिए, भीख मांगने वाले लोगों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित किया जाना चाहिए और इसे अक्सर अपडेट किया जाना चाहिए। भिखारियों की पहचान करने के लिए, नगर निगम गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम कर सकते हैं, जैसा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मानकीकृत सर्वेक्षण प्रारूपों का उपयोग करने की सिफ़ारिश में सुझाया गया है। संगठित भीख मांगने को रोकने, अपराधियों को दंडित करने और पीड़ितों को अपने पैरों पर वापस खड़े होने में मदद करने के लिए विशेष कानून लागू करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अनुशंसित जबरन भीख मांगने को अवैध बनाने के लिए कानून अपनाने से तस्करी और शोषण करने वाले संगठनों पर रोक लगेगी। लोगों को सम्मानजनक नौकरी खोजने या स्वरोजगार के अवसरों का पीछा करने में सक्षम बनाने के लिए, आश्रय गृहों को कौशल-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रम आश्रय गृहों के साथ मिलकर भिखारियों को बढ़ईगीरी, सिलाई या अन्य व्यवसायों में कौशल सिखा सकते हैं जो उनकी योग्यता के अनुकूल हों। आश्रय गृहों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएँ और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ प्रदान करें, ताकि अनुपचारित बीमारियों, व्यसन और विकलांगताओं का समाधान किया जा सके।
एनएचआरसी आश्रय गृहों को आयुष्मान भारत लाभों को एकीकृत करने की सलाह देता है, ताकि पुनर्वास से गुज़र चुके लोगों के लिए स्वास्थ्य कवरेज की गारंटी दी जा सके। बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुँच: शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत, भीख माँगने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाएँ और सुनिश्चित करें कि उन्हें खाना, कपड़े और सहायता मिले। भिखारी बच्चों के माता-पिता को लक्षित करके विशेष जागरूकता अभियान चलाकर, विशेष रूप से शहरी मलिन बस्तियों में, स्कूलों में नामांकन बढ़ाया जा सकता है। भिक्षा के बजाय पुनर्वास कार्यक्रमों में दान को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित करें। हैदराबाद जैसे शहरों में लोगों को भिखारियों के बजाय सरकारी आश्रयों में दान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सफल अभियान चलाए गए हैं। भीख माँगना भारत में व्यवस्थित उपेक्षा और संगठित शोषण का एक लक्षण है, न कि केवल ग़रीबी का प्रतिबिंब। हालाँकि बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ़ बेगिंग एक्ट, 1959 जैसे कानून ने इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन यह अक्सर अपराधियों के बजाय पीड़ितों को अपराधी बनाता है। जवाबदेही और पुनर्वास पर ज़ोर देते हुए, इंदौर में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध जैसे साहसिक क़दम उम्मीद जगाते हैं।
भारत के भिक्षावृत्ति विरोधी अभियान का लक्ष्य दंड के बजाय सशक्तिकरण होना चाहिए। नागरिकों के रूप में भीख मांगने के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को धर्मार्थ कार्यों के बजाय प्रणालीगत परिवर्तन की दिशा में क़दम के रूप में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। भीख मांगने को समाप्त करने के लिए, हमें लोगों के जीवन को सशक्त बनाना होगा। ग़रीबी के चक्र को समाप्त करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा जाल को मज़बूत किया जाना चाहिए, समावेशी शिक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए और कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक आत्मनिर्भर भारत जहाँ प्रत्येक व्यक्ति देश की उन्नति में सार्थक और सम्मानजनक योगदान देता है, भिक्षावृत्ति विरोधी कानूनों और समुदाय-संचालित पुनर्वास के सख्त प्रवर्तन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
— प्रियंका सौरभ