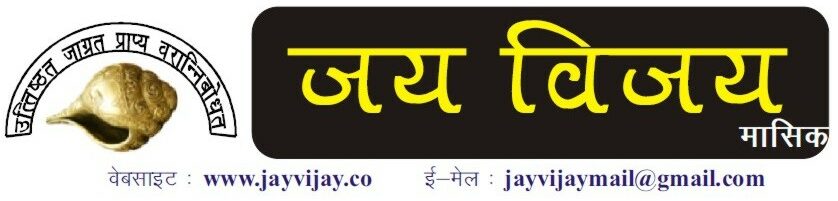छूटा पीछे पहाड़ : स्मृतियों के वातायन से आता शीतल पवन का झोंका
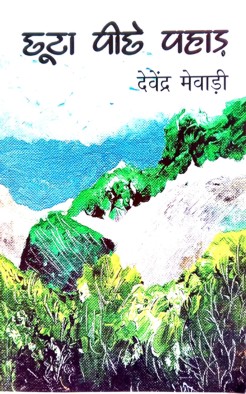 साहित्य की विविध विधाओं में संस्मरण, यात्रावृत्त एवं आत्मकथाएं पाठकों को बहुत लुभाती रही हैं। कारण कि हर कोई अपने प्रिय लेखक के जीवन और तत्कालीन देश समाज के जीवन को देखना-समझना चाहता है। एक लेखक के पास ही वह हुनर एवं कला कौशल होता है कि वह पाठक को घर बैठे अतीत की यात्रा भी कराता है और अंजुरी-अंजुरी भरकर लोक आनन्द का मधु रस भी परोसता है। स्मृतियों के सहारे वह शब्दचित्रों का एक फलक रचता-बुनता है और उस फलक में उकेर देता है बचपन के संगी-साथी, खेल, खानपान, नदी-नाले, जंगल-पहाड़, पंछी, गोरू-बछेरू। पत्तों को चूमती बहती हवा की सरसराहट और ठंडी चादर में लिपटी नदी-ताल की लहरें। शादी-ब्याह की रस्मों की मधुरता और खिलखिलाहट से गूंजते घर-आंगन और दिलों में पसरी ढोलक की थाप, गीतों की महक। संयोग के सुखद पल तो वियोग-विरह की टीस भी। पाठक उत्सुकता जगाये लेखक के साथ चलता रहता है कि अब आगे क्या होगा। और जब कोई कृति देवेंद्र मेवाड़ी जैसे सिद्ध समर्थ रचनाकार की हो तो फिर क्या कहने। ‘छूटा पीछे पहाड़’ मेरे हाथों में हैं, ऐसा लगता है कि हम किताब पढ़ नहीं रहे बल्कि एक फिल्म देख रहे हैं धीरे धीरे। पिछले दिनों, संभावना प्रकाशन, हापुड़ से छपी देवेंद्र मेवाड़ी की संस्मरण आधारित आत्मकथात्मक पुस्तक ‘पीछे छूटा पहाड़’ साहित्यकारों एवं पाठकों के मध्य चर्चा में है। पहाड़! क्या है पहाड़? पहाड़ जीवन का स्रोत है, सघन प्रेम के आधार है। समाधान का उज्ज्वल पथ है और तप साधना के बिछौने भी। पहाड़ परीक्षा है, संघर्ष है और उत्ताल उत्साह भी। पहाड़ केवल देना जानता है पानी, पवन, बादल, औषधि, भोजन, खनिज और चेतावनी भी, क्योंकि पहाड़ सहृदय है और निर्मल भी। वह अपने सीने में संजोये रहता है लोकस्वर और तमाम कथाएं भी जो रिसती रहती हैं चट्टानों से बूंद-बूंद और तब आकार लेती है कोई कृति ‘छूटा पीछे पहाड़’। वरिष्ठ साहित्यकार एवं विज्ञान कथा लेखक देवेंद्र मेवाड़ी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सात दशक से अधिक समय से पहाड़ को अपनी स्मृतियों में सहेजे वह लगातार लेखनरत हैं। प्रस्तुत पुस्तक में देबीदा अपनी जीवन यात्रा को ही एक प्रकार से पाठकों के साथ साझा करते हैं। पुस्तक पढ़ते हुए लगता है कि कोई बूढ़ा किस्सागो सामने बैठ कर अपने जीवन की किताब बांच रहा है और यह बांचना इतना स्वप्निल, चुम्बकीय और मिठास भरा है कि पाठक लेखक के पीछे-पीछे चल पड़ता है हुंकारी भरते हुए कदम दर कदम।
साहित्य की विविध विधाओं में संस्मरण, यात्रावृत्त एवं आत्मकथाएं पाठकों को बहुत लुभाती रही हैं। कारण कि हर कोई अपने प्रिय लेखक के जीवन और तत्कालीन देश समाज के जीवन को देखना-समझना चाहता है। एक लेखक के पास ही वह हुनर एवं कला कौशल होता है कि वह पाठक को घर बैठे अतीत की यात्रा भी कराता है और अंजुरी-अंजुरी भरकर लोक आनन्द का मधु रस भी परोसता है। स्मृतियों के सहारे वह शब्दचित्रों का एक फलक रचता-बुनता है और उस फलक में उकेर देता है बचपन के संगी-साथी, खेल, खानपान, नदी-नाले, जंगल-पहाड़, पंछी, गोरू-बछेरू। पत्तों को चूमती बहती हवा की सरसराहट और ठंडी चादर में लिपटी नदी-ताल की लहरें। शादी-ब्याह की रस्मों की मधुरता और खिलखिलाहट से गूंजते घर-आंगन और दिलों में पसरी ढोलक की थाप, गीतों की महक। संयोग के सुखद पल तो वियोग-विरह की टीस भी। पाठक उत्सुकता जगाये लेखक के साथ चलता रहता है कि अब आगे क्या होगा। और जब कोई कृति देवेंद्र मेवाड़ी जैसे सिद्ध समर्थ रचनाकार की हो तो फिर क्या कहने। ‘छूटा पीछे पहाड़’ मेरे हाथों में हैं, ऐसा लगता है कि हम किताब पढ़ नहीं रहे बल्कि एक फिल्म देख रहे हैं धीरे धीरे। पिछले दिनों, संभावना प्रकाशन, हापुड़ से छपी देवेंद्र मेवाड़ी की संस्मरण आधारित आत्मकथात्मक पुस्तक ‘पीछे छूटा पहाड़’ साहित्यकारों एवं पाठकों के मध्य चर्चा में है। पहाड़! क्या है पहाड़? पहाड़ जीवन का स्रोत है, सघन प्रेम के आधार है। समाधान का उज्ज्वल पथ है और तप साधना के बिछौने भी। पहाड़ परीक्षा है, संघर्ष है और उत्ताल उत्साह भी। पहाड़ केवल देना जानता है पानी, पवन, बादल, औषधि, भोजन, खनिज और चेतावनी भी, क्योंकि पहाड़ सहृदय है और निर्मल भी। वह अपने सीने में संजोये रहता है लोकस्वर और तमाम कथाएं भी जो रिसती रहती हैं चट्टानों से बूंद-बूंद और तब आकार लेती है कोई कृति ‘छूटा पीछे पहाड़’। वरिष्ठ साहित्यकार एवं विज्ञान कथा लेखक देवेंद्र मेवाड़ी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सात दशक से अधिक समय से पहाड़ को अपनी स्मृतियों में सहेजे वह लगातार लेखनरत हैं। प्रस्तुत पुस्तक में देबीदा अपनी जीवन यात्रा को ही एक प्रकार से पाठकों के साथ साझा करते हैं। पुस्तक पढ़ते हुए लगता है कि कोई बूढ़ा किस्सागो सामने बैठ कर अपने जीवन की किताब बांच रहा है और यह बांचना इतना स्वप्निल, चुम्बकीय और मिठास भरा है कि पाठक लेखक के पीछे-पीछे चल पड़ता है हुंकारी भरते हुए कदम दर कदम। ‘छूटा पीछे पहाड़’ में लेखक ने कथा कहन की एक अलग शैली चुनी है जिससे यह कृति विशेष बन गयी है। लेखक अपनी जीवन कथा मां ईजू के माध्यम से पाठक को सुना रहे हैं। एक अंश देखिए, ‘‘खरीफ का मौसम विदा होता और हम टूर पर निकल जाते, कभी हैदराबाद और कभी गुजरात में गोधरा। आज याद आते हैं, वे दिन! बताओ ना उन दिनों के बारे में? सुनोगे। तब ईजू हुंगुर (हुंकारी) देती- ओं, और कथा आगे बढ़ जाती है। यह आत्मकथात्मक आख्यान है। स्मृति के झरोखों से आते शीतल पवन के झोंके की तरह, पाठक का तन-मन तृप्त हो जाता है। पढ़ाई के लिए पहले लेखक की जन्मभूमि कालाआगर छूटी और फिर ओखलकांडा के बाद आगे के अध्ययन हेतु नैनीताल जाना हुआ। एमएससी करने के बाद वनस्पतियों एवं पशु-पक्षियों में रुचि के चलते प्रांतीय वन सेवा में जाने का निश्चय किया, दो बार चयनित हो जाने के बाद भी बुलावा न आने का दर्द भूल नये रास्ते पकड़ आगे बढ़ने का संकल्प पाठक को भी ऊर्जा से लबरेज कर देता है। नैनीताल में कहानीकार छात्र साथी लक्ष्मण सिंह बटरोही से मिलने और टी हाऊस में बैठ कहानियों पर बातें करने और एकदूसरे को अपनी कहानियां सुनाने के प्रसंग रोचक हैं। यहीं पर बटरोही ने ‘बुरांश के फूल’ लिखी तो देबीदा ने ‘दाड़िम के फूल’। यहीं साप्ताहिक ‘पर्वतीय’ में सहायक संपादक का काम भी किया। यमुनादत्त वैष्णव ‘अशोक’ के कहने पर विज्ञान गल्प लेखन की शुरुआत करते हुए ‘शैवाल’ और ‘प्रेतलीला’ नामक दो विज्ञानकथाएं भी लिखी जो छपी और सराही गयीं। नैनीताल से जीवन की धारा नई दिल्ली की ओर मुड़ी। पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में कृषि वैज्ञानिक के रूप में नौकरी करते हुए मक्का की फसल पर नवीन शोध हेतु हैदराबाद और गोधरा जाने एवं तमाम अजनबी लोगों से मिलने, नई बातें सीखने के पल रोमाचिंत करते हैं। मक्का के कीचड़ युक्त खेतों में उमस भरी गर्मी में एक-एक पौधे को गिनने, बीमार पौधे अलग करने, फूल-भुट्टों में परागण हेतु लिफाफे लगाने, पकने पर भुट्टे तोड़कर लैब में ले जाने और तमाम आंकड़ों से जूझने की रोचक घटनाएं पृष्ठों से आंखें नहीं हटने देतीं। दिल्ली तो लेखकों का जमघट, वहां के काफी हाउस में मिले तमाम साहित्यकारों यथा भीष्म साहनी, विष्णु प्रभाकर, राजेन्द्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी, प्रदीप पंत, रमेश उपाध्याय आदिक के संग बोलने-बतियाने के रोचक प्रसंगों के साथ ही गांव, खेत, पहाड़, जंगल, अनुसंधान आदि की ढेर सारी बातें सुवासित सुमनों की माला सी ही लगती है। जीवन नौका मंथगति से प्रवहमान ही थी कि समय के चप्पू ने धार काट पंतनगर की राह ली। पूसा इंस्टीट्यूट की शोध की दुनिया छोड़कर पंतनगर विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में लेखन, संपादन की जमीन तलाश काम शुरू करना, पंतनगर पत्रिका के लिए लेख, समाचार आदि तैयार करने, रात-रात भर प्रेस में काम करने, फिर किसान भारती का संपादन दायित्व पाकर किसानों से संवाद उनके अनुभवों को लिखवाना। इसी दरम्यान इंद्रासन धान की नस्ल बनाने वाले किसान इंद्रासन से भेंट, लैंटाना बग पर काम करने वाले प्राइमरी शिक्षक चंद्रशेखर लहोमी के शोध का प्रकाशन करने जैसे कार्य से पाठक परिचित होते हैं। गांव से पिता जी का पंतनगर विश्वविद्यालय आना दरअसल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक गांव या कहूं कि एक ग्राम्य संस्कृति का ही आना है अपने अनन्त अनुभवों की गठरी के साथ।
वास्तव में देवेन्द्र मेवाड़ी जी साहित्य और विज्ञान के दो किनारों को जोड़ते पुल के रूप में दिखते हैं। इस पुल से गुजरकर पाठकों की दोनों ही क्षेत्रों में खूब आवाजाही है। प्रकृति अपने पूरे विस्तार से व्यक्त हुई है तो पहाड़ी जीवन के संघर्ष, जिजीविषा एवं स्थानीय रोजगार के अभाव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। वह साहित्य की दृष्टि से विज्ञान को देखते और पाठकों को परोसते हैं, इसीलिए उसका सहज आस्वादन किया जा सकना सम्भव होता है। बकौल मेवाड़ी कि वह साहित्य की कलम से विज्ञान लिखते हैं। यही कारण है कि उनका विज्ञान लेखन सरल और तरल है। उनका लेखन विज्ञान के शोध, अनुसंधान एवं आविष्कार की वाटिका में साहित्य के महकते पुष्प खिलाता है। उस उपवन में वह अपनेपन की खाद डालते हैं और नेह का जल सिंचन। 18 शीर्षकों का ताज सजाए 211 पृष्ठों का फैलाव लिए पुस्तक ‘छूटा पीछे पहाड़’ अत्यंत सुरुचिपूर्ण एवं ताजगीभरी है। मुद्रण साफ-सुथरा, आवरण आकर्षक है। पुस्तक पठनीय एवं संग्रहणीय तो है ही, उपहार में भी दी जाने योग्य है।
कृति : छूटा पीछे पहाड़
लेखक : देवेंद्र मेवाड़ी
प्रकाशक : संभावना प्रकाशन, हापुड़
पृष्ठ : 211, मूल्य : 300/
— प्रमोद दीक्षित मलय